सुर्ख़ियों में क्यों?
हाल ही में, गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की अवधि को मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड के कुछ हिस्सों में अगले छह महीने के लिए बढ़ा दिया है।
अन्य संबंधित तथ्य
AFSPA, 1958 के विषय में
- यह एक विशेष कानून है जो कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सेना को असाधारण शक्तियां प्रदान करता है।
- उद्देश्य: इसका उद्देश्य "अशांत क्षेत्रों" में सशस्त्र बलों को अपनी गतिविधियां संचालित करने के लिए सशक्त बनाना है। अशांत क्षेत्र वे सूचीबद्ध क्षेत्र होते हैं, जहां सार्वजनिक व्यवस्था को गंभीर खतरा होता है।
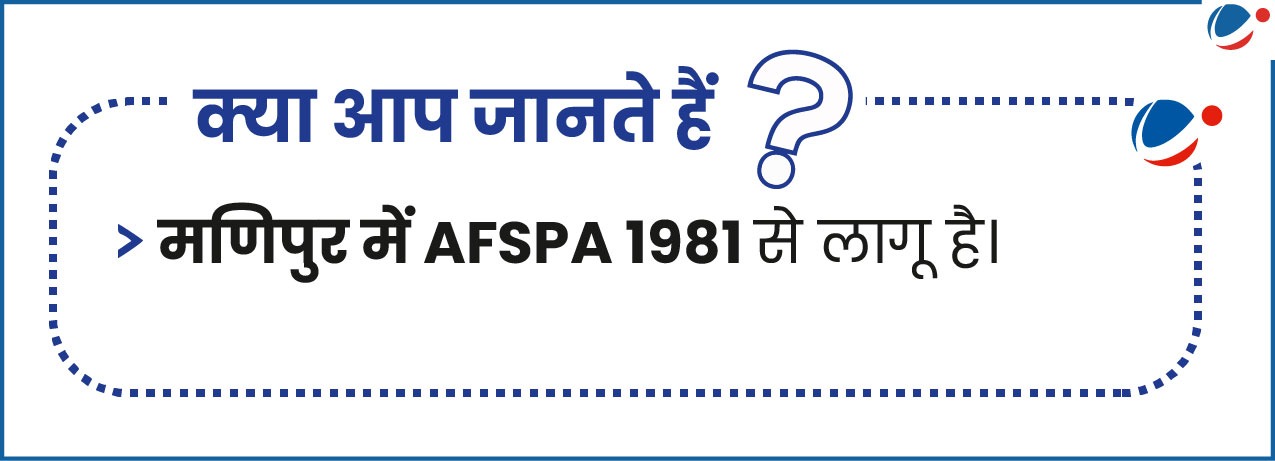
- वर्तमान में, AFSPA नागालैंड, असम, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में प्रभावी है।
- वर्ष 2015 में त्रिपुरा से, 2018 में मेघालय से और 1980 के दशक में मिजोरम से AFSPA को वापस ले लिया गया था।
- AFSPA कानून जम्मू और कश्मीर में भी प्रभावी है, जहां यह सशस्त्र बल (जम्मू और कश्मीर) विशेष शक्तियां अधिनियम, 1990 के जरिए लागू है।
अधिनियम के प्रमुख प्रावधान
- अशांत क्षेत्र की घोषणा (धारा 3): इस धारा के तहत राज्यपाल, प्रशासक या केंद्र सरकार किसी राज्य/ संघ राज्य क्षेत्र के किसी भाग या पूरे क्षेत्र को "अशांत" घोषित कर सकता है। यह घोषणा तब की जाती है, जब उन्हें लगता है कि सिविल अधिकारियों की सहायता के लिए सशस्त्र बलों की आवश्यकता है।
- सशस्त्र बलों की विशेष शक्तियां (धारा 4): यह "अशांत" घोषित क्षेत्रों में सशस्त्र बलों को विशेष शक्तियां प्रदान करता है:
- इसमें, कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ बल प्रयोग करना, यहां तक की, आवश्यकता पड़ने पर गोली चलाना भी शामिल है।
- संदेह के आधार पर बिना वारंट के किसी व्यक्ति को गिरफ्तारी करना और किसी परिसर में प्रवेश/ तलाशी लेना शामिल है।
- 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर रोक लगाना।
- हथियारों के गोदाम, किलेबंद मोर्चे जहां से सशस्त्र हमले किए जा सकते हैं, या सशस्त्र स्वयंसेवकों के किसी प्रशिक्षण शिविर को नष्ट करना।
- सशस्त्र बल कर्मियों के लिए प्रतिरक्षा (धारा 6): इस धारा के तहत केंद्र सरकार की मंजूरी के बिना AFSPA के तहत किए गए कार्यों के लिए किसी भी सुरक्षाकर्मी के विरुद्ध मुकदमा या कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती।
- गिरफ्तार व्यक्ति के साथ व्यवहार: सशस्त्र बलों द्वारा गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को "न्यूनतम संभावित देरी" के साथ निकटतम पुलिस प्राधिकरण को सौंपना आवश्यक होता है।
ऐतिहासिक न्यायिक निर्णय
- नागा पीपल्स मूवमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स बनाम भारत संघ वाद (1997): उच्चतम न्यायालय ने निर्णय में AFSPA को संवैधानिक रूप से वैध ठहराया, लेकिन बल प्रयोग और प्रतिरक्षा के उपयोग पर कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित किए।
- एक्स्ट्रा-ज्यूडिशियल एग्जीक्यूशन विक्टिम फैमिलीज़ एसोसिएशन बनाम भारत संघ वाद (2016): धारा 6 के तहत प्रदान की गई प्रतिरक्षा पूर्णतः निरपेक्ष है; अत्यधिक बल प्रयोग के मामले में सुरक्षा बलों को जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
- सेबेस्टियन एम. होंग्रे बनाम भारत संघ (1984): AFSPA में प्रतिरक्षा संबंधी प्रावधानों के बावजूद भी सुरक्षाबलों को कार्यवाहियों के लिए जवाबदेह ठहराया जा सकता है।
AFSPA का आलोचनात्मक मूल्यांकन
AFSPA के पक्ष में तर्क | AFSPA के विपक्ष में तर्क |
|
|
आगे की राह
- शक्तियों पर चरणबद्ध प्रतिबंध एवं समाप्ति: AFSPA को केवल 'अशांत' घोषित जिलों में ही लागू किया जाना चाहिए तथा जैसे-जैसे स्थिति में सुधार हो, इसकी शक्तियों को धीरे-धीरे सीमित किया जाना चाहिए।
- जवाबदेही के लिए धाराओं में संशोधन: कानून में संशोधन करके फर्जी मुठभेड़ों को रोकने के लिए प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं; गिरफ्तार व्यक्तियों को 24 घंटे के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करने और त्वरित जांच के लिए निरीक्षण तंत्र स्थापित करके प्रतिरक्षा तंत्र को सीमित करना आवश्यक है।
- वैकल्पिक पुलिसिंग: सामान्य कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए CRPF/ राज्य पुलिस का उपयोग किया जाना चाहिए; जबकि सेना को केवल अत्यधिक गंभीर संघर्षों के लिए ही आरक्षित रखा जाना चाहिए।
- मानवाधिकारों का अनुपालन: यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सैन्य अभियानों में मानवाधिकारों का सम्मान किया जाए; उग्रवाद विरोधी अभियानों में पेशेवर आचरण का सख्त अनुपालन किया जाना चाहिए।
- स्थानीय समुदायों का विश्वास एवं भागीदारी: स्थानीय जनता का समर्थन प्राप्त करने के लिए नागरिक समाज, नौकरशाही और सेना को स्थानीय विकास कार्यों में शामिल किया जा सकता है।
- कुछ समितियों की सिफारिशें:
- जीवन रेड्डी समिति (2005): AFSPA को निरस्त किया जाए; सेना की लंबे समय तक तैनाती को प्रतिबंधित करने और इसकी शक्तियों का गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 में शामिल करने का सुझाव दिया।
- द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (2007): हितधारकों के साथ परामर्श के बाद AFSPA को निरस्त किए जाने की अनुशंसा की।
- संतोष हेगड़े समिति (2013): फर्जी मुठभेड़ों की जांच की जाए; शक्तियों के दुरुपयोग पर रोक लगाई जाए।
- न्यायमूर्ति जे. एस. वर्मा समिति (2013): इसने AFSPA की तत्काल समीक्षा की सिफारिश की और कहा कि यदि सशस्त्र बलों का कोई अधिकारी महिलाओं के खिलाफ यौन हिंसा करता है, तो उसके खिलाफ सामान्य आपराधिक कानून के तहत कार्रवाई की जानी चाहिए।
निष्कर्ष
AFSPA, यद्यपि अशांत क्षेत्रों में उग्रवाद-विरोधी अभियानों के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है, किंतु यह मानवाधिकारों और जवाबदेही से जुड़ी चिंताएं भी उत्पन्न करता है। इसके दायरे को सीमित करने, निगरानी सुनिश्चित करने और स्थानीय शासन को मजबूत करने वाला एक संतुलित दृष्टिकोण अपनाकर लोकतांत्रिक मूल्यों से समझौता किए बिना सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है।




